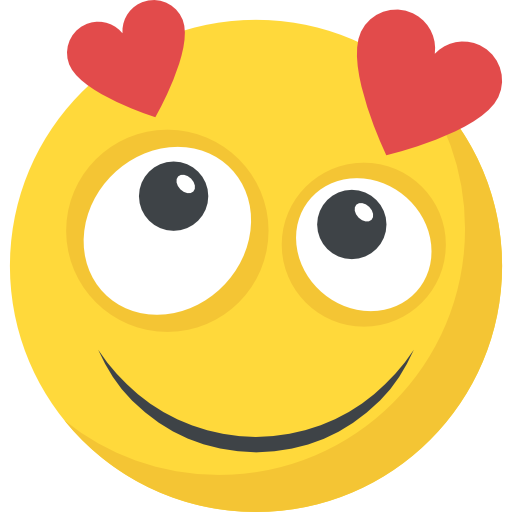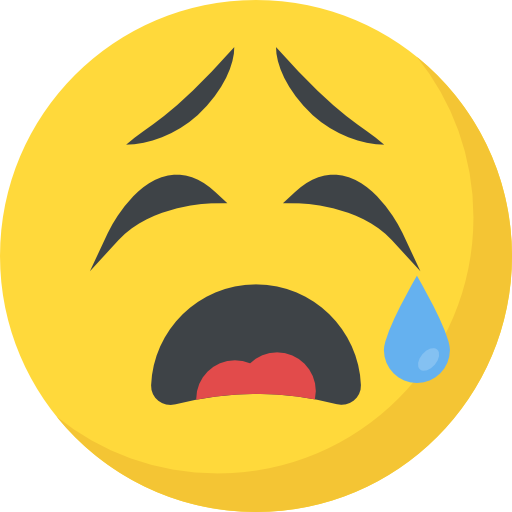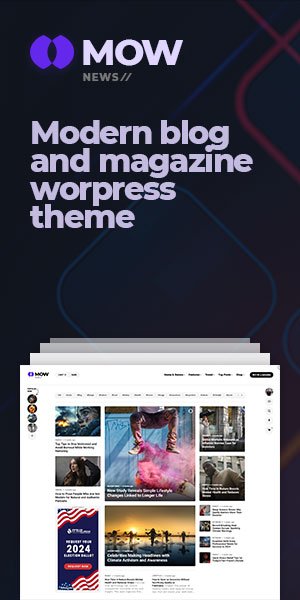Now Reading: भारत में क्यों नहीं रुक रही है जातीय हिंसा, क्या कमजोर पड़ रही समाज में बराबरी लाने की चाह?
-
01
भारत में क्यों नहीं रुक रही है जातीय हिंसा, क्या कमजोर पड़ रही समाज में बराबरी लाने की चाह?
भारत में क्यों नहीं रुक रही है जातीय हिंसा, क्या कमजोर पड़ रही समाज में बराबरी लाने की चाह?

लेखिका: रूपरेखा वर्मा
जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब प्रमुख समस्या यह नहीं थी कि विदेशी शासन-प्रशासन की जगह एक विश्वसनीय देशी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। ज्यादा बड़ी चुनौती थी एक मुकम्मल लोकतंत्र बनाने की। देश राजघरानों के प्रभाव में था। समाज राजा-प्रजा के गैर-बराबरी वाले रिश्तों का आदी हो चुका था। सामंतवाद की गिरफ़्त उस समय भी काफी मजबूत थी। नागरिक अधिकारों की चेतना जगाने और नागरिकता के अर्थ को पूरी तरह समझने का काम अधूरा और जटिल था।
पुनर्जागरण का असर: इन पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करने का साहस देश को 19वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण की चेतना से मिला। हालांकि उस काल में क्रांतिकारी आंदोलन के बजाय सुधारात्मक आंदोलन ही हुए, लेकिन इनसे उपजी चेतना ने क्रांतिकारी बदलावों की ओर बढ़ने का रास्ता साफ किया। एक ऐसी वैचारिक उथल-पुथल पैदा की, जिसने परंपरा की जड़ता और कर्मकांडीय जकड़नों को सवालों के घेरे में खड़ा करने की रवायत मजबूत की।
बदलाव की बेचैनी: लिहाजा, आजादी के वक्त देश में ऊंच-नीच से भरी, इंसानों को बेहतर और कमतर में बांटने वाली व्यवस्था को बदलने की बेचैनी थी। धर्म और संस्कृति की जड़ता को समाप्त करने और उसकी जगह व्यापक उदारवादी व्यवस्था को लाने का उछाह था। एक बेहतरीन सपना जन्म ले रहा था। इस सपने का एक हिस्सा था जाति व्यवस्था से जुड़ी अमानवीयता और गैर-बराबरी की समाप्ति और तथाकथित निचली जातियों के मानवीय अधिकारों की बहाली।
आंख की शर्म: इस सपने को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर उस समय की सत्ता के प्रयासों में कमी ढूंढी जा सकती है। लेकिन सत्ता इस सामाजिक परिवर्तन में बाधा नहीं बनी। तमाम नए विधानों के माध्यम से सत्ता ने साथ दिया। इन प्रयासों की बदौलत ही ऐसा हुआ कि सामंती युग में जाति आधारित बर्बरता की जो कहानियां आजाद भारत में पलती पीढ़ी ने सुनीं, वे उसे अजनबी समाज की करतूतें लगती थीं। आजाद देश के नागरिकों के अनुभव में वे समाप्तप्राय थीं। अगर कभी ऐसी घटना हो भी जाए तो समाज हिल जाता था। सत्ता डोलने लगती थी। तमाम बंदोबस्त करने लगती थी।
जातीय दंभ की वापसी: आज दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। पुराना जातीय दंभ पुनर्जीवित हो उठा है। जाति आधारित नफरत, हिंसा और अपमान की घटनाओं में इधर कुछ सालों में जो बढ़ोतरी हुई है और इन घटनाओं में दरिंदगी के जो बेहद शर्मनाक तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, वे दिल दहलाने वाले हैं। स्त्रियों के साथ बलात्कार के अलावा उनके शरीर के साथ पाशविकता, पुरुषों को कोड़े, जूतों, बेल्ट या लोहे की चेन से मारना, गालियां देते और मारते हुए सिर मुंड़ा के घुमाना इत्यादि।
इटावा की घटना: ऐसे ज्यादातर मामलों में हिंसाभोगी वे रहे हैं, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं और कुछ में वे जिन्हें पिछड़ा कहा जाता है। इन्हीं घटनाओं की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी है इटावा (यूपी) में हुई वह घटना, जिसमें एक पिछड़े कथावाचक का सिर मुंड़ाकर घुमाया गया क्योंकि वह किसी ब्राह्मण बहुल इलाके से न्योता पाकर वहां कथा सुनाने चला गया था।
सवाल ही सवाल: सवाल है कि इस वहशियत, गुस्से और बेखौफ सार्वजनिक हिंसा का जन्म कहां से हो रहा है? क्यों इसके सामने हमारी आवाज रुंध जाती है? क्यों वे लोग जो रात-दिन देशप्रेम का राग अलापते-अलापते अपने कंठ सुजा लेते हैं और शक्तिसंपन्न ओहदों पर भी बैठे हैं, ये सब देख नहीं रहे और देख रहे हैं तो इसे रोकने के उपाय नहीं कर रहे? जो इन स्थितियों पर व्यथित हैं और बोलते हैं, उन्हें क्यों सजा मिलती है?
लोकतंत्र का भविष्य: क्या हमारा लोकतंत्र सचमुच गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में है? एक ऐसा पीला पड़ गया पत्ता बन चुका है जो बस डाल से लटका है, अब गिरा, अब गिरा? क्या उन्नीसवीं सदी के हमारे स्वर्णिम काल और उससे उपजे स्वप्न की अंत्येष्टि कर देने का समय आ गया है और अंतिम शोकगीत लिखना ही आज हमारी नियति है?
भीड़तंत्र की जीवनरेखा: विडंबना यह है कि वे लोग और संवैधानिक संस्थाएं जिनकी तरफ हम सामाजिक सद्भाव, अमन-चैन, सुरक्षा और प्रगति के लिए देखते हैं, वे इस पूरे परिदृश्य के प्रति एकदम उदासीन और मौन नजर आते हैं। यह मौन न केवल देश-घातक है, भीड़ तंत्र की जीवनरेखा भी बन रहा है।
डर के आगे : इन सवालों के जवाब चारों तरफ बिखरे हैं, लेकिन किसी की जबान पर नहीं आ रहे। संभवतः हम उस काल में जी रहे हैं जहां जायज और जरूरी सवाल ही नहीं, उनके जवाब भी हमें डराते हैं।